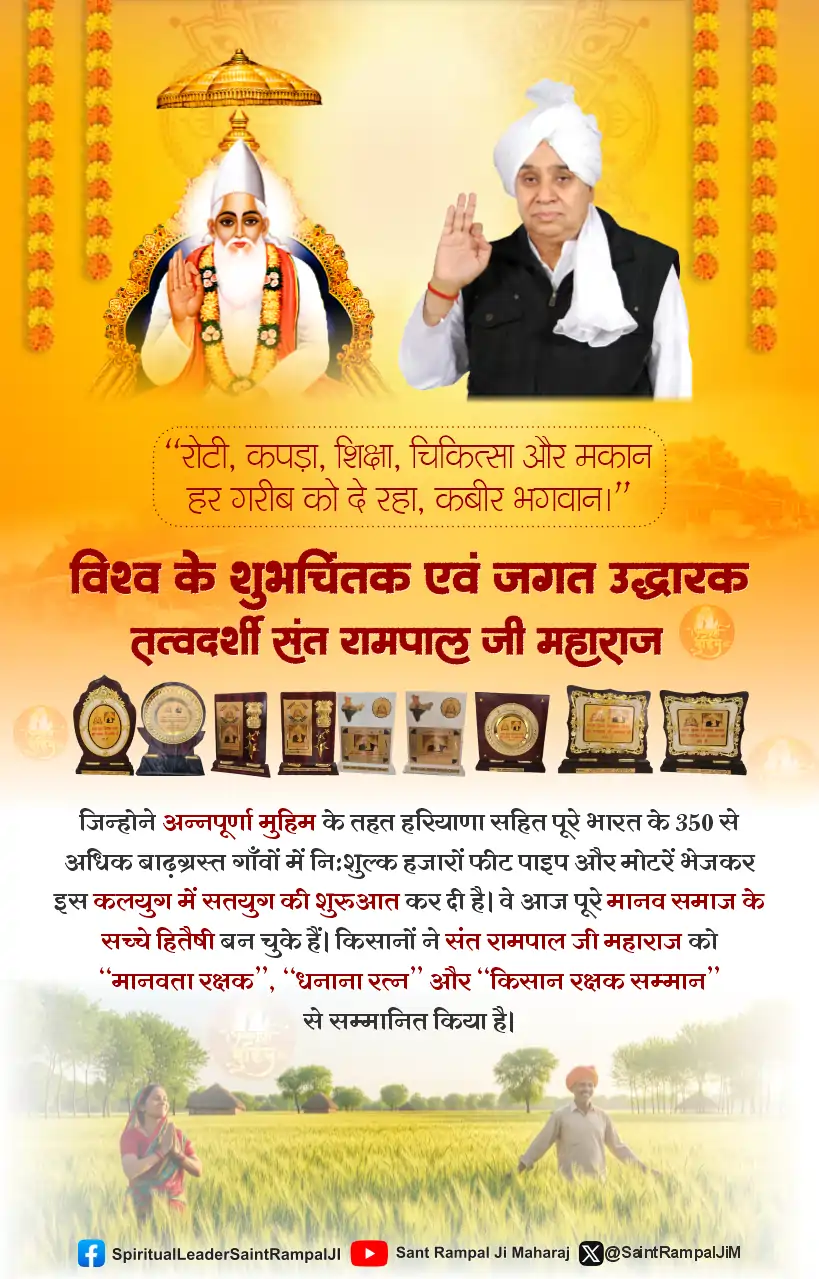टोक्यो/नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2025 – अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाते हुए, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान और चीन की अपनी चार दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की। यह यात्रा टोक्यो में उच्चस्तरीय वार्ता के साथ आरंभ हुई है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 50% का दंडात्मक टैरिफ लगाने के कुछ दिन बाद हो रही है।
ट्रंप का यह निर्णय भारत की रूसी तेल और हथियारों की निरंतर खरीदारी को लेकर लिया गया है। विश्लेषकों ने इस कदम को एक संभावित “व्यापार प्रतिबंध” बताया है जो मुख्य क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को 70% तक घटा सकता है। इसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली ने एशिया में अपनी आर्थिक साझेदारी विविधीकरण के प्रयासों को तेज कर दिया है।
टैरिफ का व्यापक प्रभाव: भारतीय उद्योग पर भारी मार
27 अगस्त को प्रभावी हुए इन टैरिफ्स में पिछली 25% दर से दोगुना इजाफा किया गया है। यह भारतीय वस्तुओं की व्यापक श्रृंखला को प्रभावित करता है, जिसमें वस्त्र, रत्न और आभूषण, जूते-चप्पल, खेल सामग्री, फर्नीचर और झींगा मछली शामिल हैं।
इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षरित ट्रंप के कार्यकारी आदेश का यह हिस्सा व्यापक “पारस्परिक टैरिफ” नीति का अंग है। व्हाइट हाउस का मानना है कि इससे अमेरिकी घाटे में योगदान देने वाली अनुचित व्यापार प्रथाओं को सुधारा जा सकेगा। इस निर्णय ने वैश्विक बाजारों में हलचल मचा दी है।
भारतीय अधिकारियों ने घरेलू उद्योगों से आत्मनिर्भरता पर ध्यान देने और वैकल्पिक बाजारों की खोज करने का आग्रह किया है। इसके जवाब में मोदी ने जोर देकर कहा है कि जापान और चीन की उनकी यात्राएं “राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाएंगी और वैश्विक शांति एवं स्थिरता में योगदान देंगी।”
जापान शिखर सम्मेलन:रणनीतिक संबंधों का मजबूतीकरण
मोदी का कार्यक्रम टोक्यो से शुरू हुआ, जहां वे शुक्रवार की सुबह जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार और अवसंरचना पर व्यापक चर्चा की।
वार्ता का समापन “हमारी अगली पीढ़ी की सुरक्षा और समृद्धि के लिए साझेदारी” शीर्षक से एक संयुक्त बयान के साथ हुआ। मुख्य घोषणाओं में जापान का अगले पांच वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन (लगभग 34 बिलियन डॉलर) का निवेश करने का वादा शामिल है। यह निवेश सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर केंद्रित होगा।
चंद्रयान-5 मिशन: अंतरिक्ष सहयोग की नई उड़ान
एक उल्लेखनीय घोषणा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) के बीच चंद्रयान-5 चंद्र मिशन के लिए सहयोग की थी। इसका उद्देश्य संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देना है।
शिखर सम्मेलन में भारत के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के चल रहे विकास पर भी चर्चा हुई। जापान ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को तेज करने की प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा सहयोग में प्रमुखता से चर्चा हुई, जिसमें मानवरहित भूमि वाहनों के सह-विकास और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर समझौते शामिल हैं।
चीन के साथ नाजुक संतुलन: एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारी
टोक्यो से मोदी 31 अगस्त को चीन के तियांजिन जाने वाले हैं। वहां राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा आयोजित वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सात वर्षों में मोदी की चीन की पहली यात्रा है। पिछली बार वे 2018 में वुहान अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लिए गए थे।
यह यात्रा सीमा विवादों और 2020 की गलवान घाटी की झड़प की पृष्ठभूमि में हो रही है, जिसने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया था। हालांकि, ट्रंप की टैरिफ घोषणा के महज कुछ दिन बाद इसका समय इस अटकलबाजी को बढ़ावा दे रहा है कि भारत आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए बीजिंग के साथ संबंधों को रीसेट करना चाह रहा है।
रूस और चीन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की संभावना
शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक बैठकों की आशा की जा रही है। इन चर्चाओं में व्यापार विविधीकरण, सीमा स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर फोकस होगा। चीन ने पहले ही अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के रुख का समर्थन किया है। चीनी राजकीय मीडिया ने ट्रंप की नीतियों की “एकपक्षीय धमकी” के रूप में आलोचना की है।
चर्चाओं में दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष उड़ानों को फिर से शुरू करना और गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाना शामिल हो सकता है। भारत का लक्ष्य चीन के साथ 100 बिलियन डॉलर के व्यापारिक घाटे को कम करना है।
बहुध्रुवीय कूटनीति: व्यापक रणनीति का हिस्सा
यह कूटनीतिक पहुंच ट्रंप की आक्रामक व्यापार नीतियों के लिए भारत की व्यापक प्रतिक्रिया का हिस्सा है। हाल के हफ्तों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने मास्को में पुतिन से मुलाकात की और रूसी नेता की भारत यात्रा को अंतिम रूप दिया। मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ बातचीत की।
ब्राजील के उपराष्ट्रपति अक्टूबर में भारत आने वाले हैं। चीन ने टैरिफ के खिलाफ नई दिल्ली का सार्वजनिक समर्थन किया है। यहां तक कि इजरायल भी शामिल हुआ है, भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की है।
आर्थिक चुनौतियां और वैश्विक प्रभाव
विश्लेषकों का चेतावनी है कि टैरिफ से अमेरिकी परिवारों पर सालाना औसतन 1,300 डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो सकती हैं। भारत के लिए निर्यात पर मार – जिसका अनुमान 10-15 बिलियन डॉलर है – एशिया और उभरते बाजारों की ओर रुख करना आवश्यक बनाता है।
सिंगापुर की एस राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के दक्षिण एशिया विशेषज्ञ डॉ राजेश बसरूर का कहना है, “जापान के निवेश भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देकर टैरिफ के कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं।”
टोक्यो के एक बिजनेस फोरम में मोदी के संबोधन में “लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों” पर जोर दिया गया, जो एशिया के आर्थिक परिदृश्य में भारत को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने के इरादे का संकेत देता है।
चुनौतियां और आलोचनाएं: संतुलन की कला
हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत की सावधान रणनीति जापान को नाराज नहीं करना चाहती – जो अमेरिका का सहयोगी है – जबकि लद्दाख में चल रहे सैन्य गतिरोध के बीच चीन के साथ संबंधों को संभालना भी जरूरी है।
भारत में विपक्षी आवाजों सहित आलोचकों का सवाल है कि क्या यह “पैनिक मैनेजमेंट” अमेरिकी सद्भावना पर अत्यधिक निर्भरता को उजागर करता है। फिर भी समर्थक इसे व्यावहारिक कूटनीति बताते हैं, जिसमें संरक्षणवाद के खिलाफ ब्रिक्स एकता को मजबूत करने की क्षमता है।
एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के विदेश नीति विशेषज्ञ सी राजा मोहन कहते हैं, “मोदी की यात्राएं एक बहुध्रुवीय दृष्टिकोण का संकेत देती हैं: क्वाड गठबंधनों को एससीओ सहभागिता के साथ संतुलित करना।”
निष्कर्ष: नए युग की शुरुआत
जैसे ही मोदी जापान में अपनी यात्रा समाप्त करके चीन की ओर रवाना होने वाले हैं, दुनिया देख रही है कि क्या यह एशियाई रणनीति भारत को ट्रंप के व्यापारिक तूफान से बचा सकती है। महामंदी के बाद से वैश्विक टैरिफ अपने उच्चतम स्तर पर हैं, ऐसे में आर्थिक लचीलेपन और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिए दांव कभी इतने ऊंचे नहीं रहे।
इन शिखर सम्मेलनों के परिणाम एक खंडित वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। यह यात्रा न केवल तत्काल आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता स्थापित करने के लिए भी है।